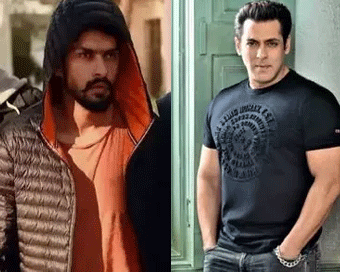एक असंभव संभावना
जब कांग्रेस मुक्त भारत के घोषित नारे के साथ भाजपा नेतृत्व काम कर रहा है, और कांग्रेस को ही नहीं उसकी चुनी हुई सरकारों को निशाना बना रहा है.
 एक असंभव संभावना |
तो आज न कल भाजपा या संघ मुक्त भारत का नारा भी लगना ही था. यह और बात है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री और हाल के चुनाव में भाजपा को पटखनी देने वाले नीतीश कुमार ने यह नारा दिया तो भाजपा की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई और गैर-भाजपाई दलों ने भी कोई बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं दी है. पर इस नारे ने जो सुगबुगाहट पैदा की है, उससे यह संभावना जगती है कि ढंग से काम हो तो ऐसा कोई मोर्चा बनाना संभव है.
उससे भाजपा और संघ को भारत से गायब किया जा सकता है,या नहीं यह बड़े विवाद का विषय हो सकता है, पर खुद बिहार के अनुभव ने साबित किया है कि भाजपा-विरोध के नाम पर गैर-भाजपाई दलों को एक मोर्चे पर लगाया जा सकता है. और अगर यह काम हो जाए तो भाजपा की साम-दाम-दंड-भेद की नीति भी काम नहीं कर पाती. फिर मुलायम, ओवैसी, पप्पू यादव, मांझी, नागमणि, कै. निषाद जैसे लोग भी सारा जोर लगाकर गैर-भाजपा वोटों का विभाजन नहीं कर सकते.
पर यह बात ऊपर से जितनी आसान लगती है, राजनैतिक रणक्षेत्र के हिसाब से उतनी ही मुश्किल है.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत, रणनीति, समर्पण और हर हाल में खुद को बचा-बढ़ा लेने की क्षमता का जवाब अगर देश के किसी दल या नेता में होता तो आजादी की लड़ाई तक हाशिये की ताकत रहा संघ आज सत्ता के सारे सूत्र हाथ में लेकर नहीं बैठा होता. एक विदेशी विचार, एक विदेशी ढंग के संगठन और भारतीय समाज की बुनियादी विविधता में जरा भी भरोसा न रखने वाला संगठन आज अगर खुद को राष्ट्रवाद, देशप्रेम और भारतीयता का चैम्पियन बताने लगा है, एक साथ हिटलर और यहूदी इस्रइल के प्रति प्रेम जगा दे रहा है, तो यह महज जादूगरी या धोखा नहीं है.
उसके पास आज सबसे बड़ी ‘फौज’ है, जो अपने संगठन के इशारे पर कुछ भी कर सकती है-एक से एक मुश्किल काम और एक से एक घटिया काम. जहां कोई नहीं जाने की हिम्मत करता है, वहां भी संघ के स्वयंसेवक सेवा भाव से पहुंच जाते हैं, तो राष्ट्रवाद और हिन्दू प्रेम के नाम पर दूसरों की जान लेने का अपराध भी कर सकते हैं, किसी स्टेंस को जिंदा जला सकते हैं, कभी कथित लव जिहाद को सबसे बड़ी समस्या बना सकते हैं.
पर आज अगर संघ मुक्त भारत के नारे पर चर्चा करने की जरूरत दिख रही है, तो सिर्फ संघ के कामों के चलते ही नहीं. इसका बड़ा कारण नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता द्वारा इसका आह्वान करना है. नीतीश ने न सिर्फ बिहार में हारी हुई बाजी पलटी है, बल्कि अपने कामकाज और व्यवहार से देश में काफी यश कमाया है. आज वे मोदी विरोधी कुल राजनीति के तीन-चार नामों में एक हैं, जिनसे देश काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं. और उनके साथ यह भी अच्छी बात है कि वे केंद्र में मंत्री रहे हुए हैं, और अभी उनकी छवि पर कोई दाग नहीं है.
अगर बहुत आगे बढ़कर भी कहा जाए तो यह कह सकते हैं कि बिहार से बाहर भी उनको चाहने वाले हैं-कुछ बिरादरी के नाम पर, कुछ मंडल नाम पर और कुछ पुरानी समाजवादी धारा के नाम पर. उनके जैसी छवि संभवत: ममता बनर्जी और नवीन पटनायक जैसे गिनती के लोगों की है-कुछ-कुछ लेकिन परंतु के साथ. अभी विपक्षी राजनीति के धुरी बने राहुल गांधी भी नीतीश के मुकाबले कम विसनीय लगते हैं-उन्होंने अभी तक कुछ प्रदशर्न करके नहीं दिया है. पार्टी संगठन और एक अखिल भारतीय मौजूदगी के मामले में तो वे नीतीश से आगे हैं, पर चमक नीतीश में ज्यादा है.
नीतीश की राजनीति ही बाधा
लेकिन खुद नीतीश ने अब तक चार दशक से ज्यादा की जो राजनीति की है, वही इस काम में सबसे बड़ी बाधा बनने जा रही है. मुश्किल इस बात से खास नहीं होगी कि वे जमाने तक एनडीए का हिस्सा रहे या उन्होंने बिहार में संघ को हाथ-पांव फैलाने का अवसर दिया या फिर मौका-बेमौका खुद भी संघ की तारीफ करते रहे हैं. ये चीजें राजनीति में बहुत ज्यादा असर नहीं करतीं, खासकर तब जब आज वे संघ या भाजपा विरोधी राजनीति के मोर्चे पर डटे सबसे प्रमुख लोगों में दिखाई दे रहे हैं. नीतीश की मुश्किल उनका संगठन पर ध्यान न देना और पार्टी के अंदर भी इस काम के लिए किसी काबिल आदमी पर भरोसा करके उसे जिम्मा न सौंपना है.
हम जानते हैं कि उन्होंने भाजपा विरोधी तेवर तभी अपनाया जब संजय जोशी ने उनके एक दर्जन से ज्यादा नाराज सांसदों की बैठक की. किसी भी वक्त उनके आधे सांसद उनसे नाराज ही दिखते हैं. पार्टी संगठन का जिम्मा ही उन्होंने जिस वशिष्ठ नारायण सिंह को दिया है. वे खुद उनसे काफी नाराज थे और उन्हें भी कुशल संगठनकर्ता नहीं माना जाता. अभी केसी त्यागी उनकी तरफ से बाकी दलों से बात करते हैं, या प्रशांत किशोर रणनीति बनाते बताए जाते हैं. ये दोनों ही कितने विस्त हैं, या नीतीश इन पर कितना भरोसा करते हैं, यह मानना मुश्किल है.
बात एक चुनाव लड़ने या विास मत जीतने जैसी होती तब तो संघ मुक्ति का कर्मकांड जरूर पूरा हो जाता. पर जब मुकाबला स्वयं संघ से हो तो आपको इस रवैये से काम नहीं करना होगा. और इस उमर और लत तक पहुंच कर नीतीश अब बड़े कुशल संगठनकर्ता बन जाएंगे और हजारों लोगों पर भरोसा करने लगेंगे या संगठन में लगे हजारों लोग उन पर भरोसा करने लगेंगे, यह मान लेना गलत होगा. भारत जैसे बड़े देश में प्रभावी संगठन चलाने में सैकड़ों-हजारों नहीं लाखों भरोसेमंद लोग चाहिए और जब मुकाबला संघ से हो तब अनुशासन, संगठन के प्रति निष्ठा, समर्पण और प्रतिबद्धता की जरूरत होगी क्योंकि दूसरे पक्ष के पास यह सब है.
आप अपनी विचारधारा या राजनीति में इक्कीस हो सकते हैं, पर आपका इतिहास संघ के हाथों बार-बार पिटने का ही है. और आप जिस ताकत को संघ मुक्ति के काम में लगाना चाहते हैं, उसमें से काफी बड़े लोगों को तो अपने परिवार और खजाने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं. संघ के लोगों पर दंगा फैलाने के, अफवाह उड़ाने के आरोप लगे होंगे पर पैसा उड़ाने और अपने परिवार को ही सारी प्रतिभा का खजाना समझने का दोषी नहीं बताया जा सकता. और मुश्किल यह है कि ऐसे सारे नेता और उनके घरेलू दल खुद को नीतीश और उनकी पार्टी से कम नहीं समझते.
आजमाये सूत्र में वह धार नहीं
छवि और अच्छे कामकाज के रिकॉर्ड के साथ एक और चीज है, जो उनको भी बल दे रहा होगा और बाकी लोगों को भी उनकी बातों में दम देखने का एक कारण. यह चीज है डॉ. लोहिया का गैर-कांग्रेसवाद. साथ के दशक की कांग्रेस संगठन ही नहीं विचारों और हर मामले में संघ से मजबूत स्थिति में थी. खुद डॉ. लोहिया उसकी तुलना विशाल बरगद से करते थे. वे कुछ ज्यादा हड़बड़ी में थे, और इस रणनीति को दीकालिक की जगह दरम्यानी राजनीति ही मानते थे.
उनकी मुहिम कम समय में ही सभी गैर-कांग्रेसी दलों को साथ ले आई थी, और कम से कम उत्तर भारत में कांग्रेस की जड़ें हिलाने में कामयाब रही थी. पर तब यह भी था कि संसद में आधे दर्जन से भी कम सांसदों वाली उनकी पार्टी ने मुख्य विपक्ष की भूमिका ले ली थी, और चीन से मिली पराजय के सवाल पर नेहरू सरकार के पसीने छुड़ा दिए थे. कमजोर या मजबूत समाजवादियों का पूरे देश में वजूद था. आज जनता दल के दो दर्जन से ज्यादा सांसद वेतन भत्ते लेने के अलावा कुछ करते भी हैं, यह समझना मुश्किल है. और जब कोई सक्रिय होता भी है, तो नेतृत्व के पेट में दर्द होने लगता है.
पर यह भी याद रखना होगा कि गैर-कांग्रेसवाद और सांप्रदायिकता-विरोध की राजनीति का अत्यधिक दोहन भी हुआ है, और इसका आकषर्ण घटा भी है. लोहिया ने गैर-कांग्रेसवाद का सूत्र बरगद बन बैठी और घटिया संस्कृति का प्रतीक बन गई कांग्रेस को सत्ता से हटाने के मंत्र के तौर पर दिया था.
साथ ही, यह भी कहा था कि यह दरमियानी रणनीति है. अब तक इस सूत्र का बहुत दोहन हो चुका है. सांप्रदायिकता-विरोध के खेल का भी अत्यधिक दोहन हुआ है, और इसमें भी बहुत दम नहीं बचा है. इसका दम यही रह गया है कि गुजरात दंगों के लिए अभी भी अफसोस न करने वाले नरेन्द्र मोदी को आगे होने से मुसलमान भाजपा से बिदक ही रहे हैं. वे और मोदी को हरा सकने वाली ताकत पर एकजुट होंगे. सो, अब विपक्षी एकता बनाने वाले इन्हीं सूत्रों और हथियारों से काम हो जाएगा, यह सोचना गलत होगा.
पहले पच्चीस साल से पिछड़ों की ऊर्जा को अपने निजी और पारिवारिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की माफी मांगने के साथ प्रायश्चित का काम भी करना होगा. मुल्क में पच्चीसेक सालों से चल रही अर्थनीति की सही आलोचना और विकल्प पेश करने से भी काम होगा जो नीतीश बिहार के सर्वसमावेशी विकास के नाम से कर रहे हैं. यह सही है कि आज की राजनीति के सभी लोग इस नई अर्थनीति को लाने में कुछ न कुछ जिम्मेवार हैं-पर मुख्य भूमिका कांग्रेस और भाजपा या वि बैंक-आईएमएफ से जुड़े अर्थशास्त्रियों की ही थी. हम भी अपने कथित समाजवादी नीति और लाल फीताशाही से त्रस्त थे. आज भाजपा की सरकार और उसके पीछे संघ और तेज उदारीकरण की नीतियां चला रही है.
अब अगर गरीबों-आदिवासियों-दलितों, अकलियतों और पिछड़ों की, गांव की खेती-किसानी की जरूरतों को आगे करके कोई वैकल्पिक सूत्र विकसित किए जाएं तो मजे से मंडल नाम से निकली शक्ति-ऊर्जा को और कमजोरों-गरीबों के संघर्ष से जुड़ी ताकतों को एकताबद्ध किया जा सकता है. उस ताकत को आप संघ-विरोध अर्थात सांप्रदायिकता को खत्म करने में लगाएं या नई सोच वाली अर्थनीति में तभी कल्याण होगा.
| Tweet |