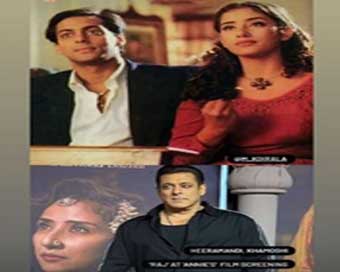अंग्रेजी की गुलामी से नहीं आएंगे अच्छे दिन
भारत की शासन व्यवस्था अंग्रेजों ने उन हाथों में सौंपी थी जो सदा अंग्रेजों और अंग्रेजियत से अपने को रंग कर खुद को श्रेष्ठ मानते थे.
 अंग्रेजी की गुलामी से नहीं आएंगे अच्छे दिन |
वे यही अभिलाषा रखते थे कि उन्हें बाकी ‘इंडियंस’ से अलग माना जाए. अर्थ स्पष्ट था, उन्हें विशिष्ट माना जाए. इनका वश चलता तो यह भाषाई रंगभेद सदा कायम रखते, यानी बड़े साहब तो वही बन सकते हैं जो न केवल अंग्रेजी में प्रवीण हों वरन् अंग्रेजियत की श्रेष्ठता से अभिभूत भी हों. आज के युवाओं को शायद उस संघर्ष की पूरी जानकारी न हो जिसके कारण ही भारतीय भाषाओं में 1989 से सिविल सेवा परीक्षा हो रही है. संवैधानिक आरक्षण के साथ मिलाकर इसे देखें तो स्पष्ट होगा कि इसी कारण ग्रामीण, जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी भी धीरे-धीरे बढ़ती संख्या में संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षाएं उत्तीर्ण करते रहे हैं.
इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि शासन और प्रशासन का एक वर्ग इसे खतरे के रूप में देखने लगा था. वे इसे भले ही स्वीकार न करें, मगर परिस्थितिजन्य साक्ष्य यही इंगित करते हैं. 2011 के बाद अंग्रेजी माध्यम से इतर भाषाओं में परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की संख्या लगातार घटी है. आश्चर्य यह है कि यूपीएससी, जिसके पास सारे आंकड़े तथा विश्लेषण और निष्कर्ष उपलब्ध थे, क्यों सोता रहा और उसने स्वयं इस व्यवस्था में परिवर्तन करने की जरूरत क्यों महसूस नहीं की?
इसके खिलाफ देश के अनेक भागों में युवा सड़क पर उतरे, उन्होंने प्रदर्शन किए. इस दौरान उन्हें पुलिस तथा प्रशासन लाठियां और गालियां मिलीं. सवाल है कि एक स्वतंत्र, सार्वभौमिक सत्ता-संपन्न राष्ट्र, जिसके पास अनेक सक्षम भाषाओं और साहित्य का अद्वितीय भंडार हो, अपने युवाओं को अपनी भाषा में अपनी योग्यता को सिद्ध करने से वंचित करेगा? भारत में यही हो रहा है. आश्चर्य होता है जब कहा जाता है कि बिना अंग्रेजी जाने प्रशासन व्यवस्था चल ही नहीं सकती!
आज से छह दशक पहले जब सोवियत संघ का उपग्रह अंतरिक्ष में गया तो अमेरिका में तहलका मचा. रूसी अपनी भाषा के जरिए प्रगति कर रहे थे, उनके शोध के जर्नल रूसी में छपते थे. अमेरिकी व्यवस्था को उन्हें अंग्रेजी में अनुवाद कराना पड़ा. क्या जापान ने अपनी भाषा त्याग दी है? आश्चर्य यह होता है कि इन तथ्यों से सभी नीति-निर्माता वाकिफ हैं, मगर वे संभवत: प्रतिस्पर्धा को सीमित ही रखना चाहते हैं. नीतिगत स्तर पर अंग्रेजों के शासनकाल से चली आ रही निरंतरता के दुष्प्रभाव अभी चर्चा में पूरी तरह नहीं आए हैं.
पब्लिक स्कूलों के नाम से जाने जाने वाले निजी स्कूल बच्चों को पहले दिन से ही अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा देते हैं. कोई भी शिक्षाविद, वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक इसे प्राथमिक स्तर पर कतई सही नहीं मानता है. मगर अच्छे पद, अच्छी नौकरी तथा ऊंचे वर्ग में स्वीकार्यता की चकाचौंध में माता-पिता बच्चों पर यह अनावश्यक बोझ लगातार डालते जा रहे हैं. क्या विश्वास करने योग्य है कि युवा माता-पिता आपस में तय करें कि वे घर में केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चे की अंग्रेजी की प्रवीणता निर्बाध बढ़ती रहे. ऐसा चलन बढ़ रहा है.
अब उस बच्चे की बात लीजिए जो झाबुआ, कोरापुर या क्योंझार के टूटे-फूटे स्कूल में कभी-कभी आने वाले अध्यापकों से शिक्षा प्राप्त करता है और आगे बढ़ते हुए स्नातक हो जाता है. नए-नए सपने लेकर बड़े शहर आने पर वह देखता है कि जब तक उसे अंग्रेजी नहीं आएगी, केवल कागजों पर दरवाजे उसके लिए खुले हैं लेकिन पैरों में भाषा की जंजीर बंधी है. ऐसे में जो हीनभावना उसमें पैदा होगी, उसका अनुमान तो वह स्वयं तथा भुक्तभोगी परिवार ही लगा पाएगा.
1968-70 के आसपास तक ग्रामीण इलाकों के करोड़ों बच्चे इसलिए स्कूल छोड़ देते थे क्योंकि वे कक्षा में ‘अंग्रेजी में फेल हो जाते थे.’ डॉ. राम मनोहर लोहिया जैसे लोग, जो भारत की ग्रामीण तथा जनजातीय व्यवस्था को न केवल जानते थे मगर संवेदनात्मक स्तर पर उसे समझते थे, आगे आए और उनके प्रयत्नों से बिना अंग्रेजी के कक्षा दस पास करना संभव हुआ. मगर दूसरी तरफ सत्ता और निर्णय लेने के अधिकार तो उन्हीं के पास रहे जो नई दिल्ली तथा वहां के कुछ स्कूलों को भारत मान लेते हैं. इनमें कुछ का वश चले तो वे ऑक्सफोर्ड, या कैम्ब्रिज की पूरी नकल यहां पर स्थापित कर दें.
जिस युवा की पूरी शिक्षा मातृभाषा में हुई हो, जिसे अंग्रेजी पढ़ने का अवसर न मिला हो, वह उस हमवयस्क के समक्ष अंग्रेजी में प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकता है जिसने नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय तक इसी भाषा के माध्यम से शिक्षा पाई हो. अनेक तर्क दिए जा रहे हैं कि सी-सैट प्रश्नपत्र में अंग्रेजी का स्तर तो कक्षा दस के भी नीचे का है. तथ्य तो दूसरा ही है- मातृभाषा वाले का आत्मविास तो संघ लोकसेवा आयोग की नीतियों ने पहले से ही योजनाबद्ध ढंग से छीन लिया है.
अनेक प्रत्याशियों ने, जो भाग्यशाली थे तथा साक्षात्कार तक पहुंचे, अपने को अत्यंत असमंजस में पाया जब उनसे साक्षात्कार में उत्तर अंग्रेजी में देने को कहा गया. ऐसा प्रत्याशी तो असफल घोषित हो ही जाएगा. और यह तब हो रहा है जब आईएएस में उत्तीर्ण तमिलनाडु का युवा बिहार में हिंदी सीखता है, नाम कमाता है; और राजस्थान में चयनित युवा तमिलनाडु में तमिल सीखता है और सारा कार्य विश्वासपूर्वक करता है.
बड़े परिवेश में देखें तो क्या यह हर युवा का जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार नहीं है कि वह अपनी पूरी शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्राप्त करे तथा उसकी प्रतिभा का मूल्यांकन भी उसी भाषा में हो? चयनित होने के बाद प्रशिक्षण होता है- उसमें भाषागत प्रवीणता मातृभाषा के अलावा अंग्रेजी में भी दी जा सकती है. फिर चयन प्रक्रिया में भेदभाव क्यों? यह यूपीएससी का उत्तरदायित्व है कि वह सबको समान अवसर देने वाली परीक्षा व्यवस्था देश के समक्ष रखें. अंतत: भारत सरकार को संविधान की आत्मा का संरक्षण करना ही होगा.
यह कहना कठिन है कि कितने नीति-निर्धारकों ने कभी हिंद स्वराज को जाना, पढ़ा या समझा हो. उसमें से अनेक अंश हमारी समझ बढ़ा सकते हैं. इसे देखें, ‘जिस शिक्षा को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया है, वह हमारा सिंगार बनती है, यह जानने लायक है कि उन्हीं के विद्वान कहते रहते हैं कि इससे यह अच्छा नहीं है, वह अच्छा नहीं है. वे जिसे भूल से गए हैं, उसी से हम अपने अज्ञान के कारण चिपके रहते हैं. उनमें अपनी भाषा की उन्नति करने की कोशिश चल रही है. वेल्स इंग्लैंड का छोटा परगना है.
उसकी भाषा धूल जैसी नगण्य है. ऐसी भाषा का अब जीर्णोद्धार हो रहा है. वेल्स के बच्चे अपनी भाषा में बोलें, ऐसी कोशिश चल रही है. और हमारी दशा कैसी हो? हम एक -दूसरे को पत्र लिखते हैं तब गलत अंग्रेजी में लिखते हैं.’ गांधी जी यहीं नहीं रुके. उन्होंने आगे लिखा, ‘अंग्रेजी शिक्षा से दंभ, राग, जुल्म वगैरह बढ़े हैं. अंग्रेजी शिक्षा पाए लोगों ने प्रजा को ठगने में, उसे परेशान करने में कुछ भी उठा नहीं रखा है.’ इस उद्धरण को यहां देने का आशय किसी भाषा या व्यक्ति पर आक्षेप करना न तब रहा होगा, न अब हो सकता है.
फिर भी इस समय देश में, प्रशासन में अहंकार भ्रष्टाचार, अत्याचार जिस स्तर पर है, वह यह तो इंगित करता है कि चयन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है. गांव-देहात, पिछड़ों, जनजातियों से ऐसे युवा आएं जो वहां की भाषा धरोहर, साहित्य, ज्ञानार्जन परंपरा से परिचित हों, उसी में रचे-बसे हों. क्या यूपीएससी की पुनर्रचना आवश्यक नहीं हैं कि वहां नामी-गिरामी विद्वान, साहित्यकार, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक पूरे सम्मान के साथ बैठें और निर्णय लें. प्रशासनिक अधिकारी उनके निर्देशों का पालन करें.
युवाओं के आंदोलन का दायरा विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए. मैं उस भारत की कल्पना नहीं करना चाहता हूं जहां सारी भारतीय भाषाएं अंग्रेजी की चेरी बना दी जाएं. इस समय जो युवा संघर्ष कर रहे हैं वे देश निर्माण और प्रगति की अवधारणा के एक बड़े पक्ष को उजागर कर रहे हैं, जो मात्र परीक्षा तक सीमित नहीं हैं.
(लेखक एनसीईआरटी के निदेशक रहे हैं)
| Tweet |